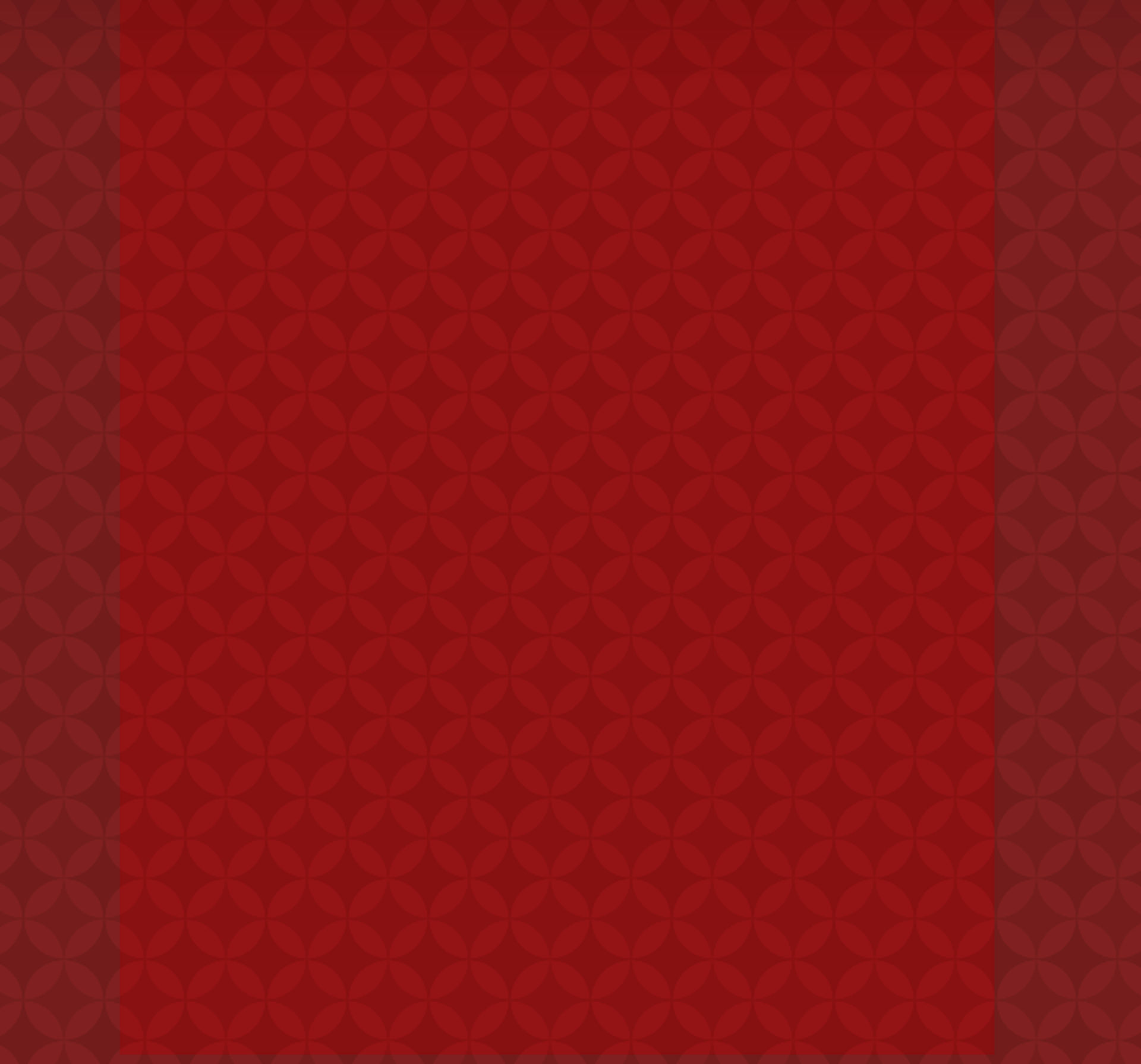खंड 2: क्यों पिछड़ गया भारत — जब सब कुछ था, फिर भी कुछ नहीं बदला?
जिस देश की मिट्टी में सोना उगता है, जहाँ नदियाँ वेद गाती हैं, जहाँ सूर्य सबसे पहले नमस्कार करता है — वहाँ आज भी भूख, बेरोज़गारी और असमानता का अंधकार क्यों है?
विश्लेषण / विचारधारा
रोहित थपलियाल
7/20/20251 मिनट पढ़ें

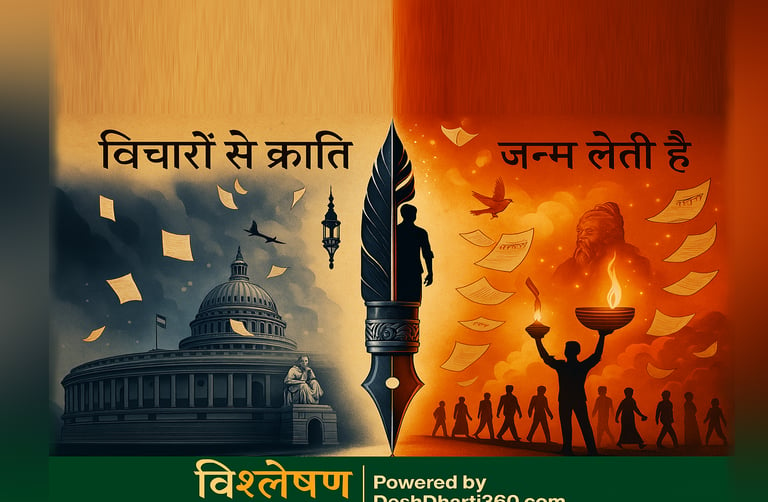
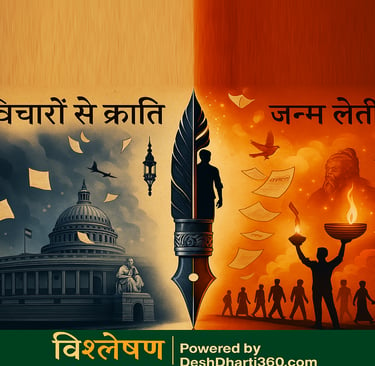
"जब नेतृत्व सेवा छोड़ दे, और स्वार्थ अपना ले
तब राष्ट्र की आत्मा घायल हो जाती है।"
भारत के पास सब कुछ था: साधन, संस्कृति, समझ और संकल्प। फिर भी हम पिछड़ गए — और यह पिछड़ना केवल आर्थिक नहीं था, यह चरित्र और चेतना का पतन था।
आज का भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ लोग पूछते हैं: “हम इतना कुछ होने के बाद भी इतना असहाय क्यों हैं?” उत्तर सीधा है — क्योंकि हमारी राजनीति नेतृत्व नहीं, नेतागिरी बन गई। नेता अब विचारधारा से नहीं, जाति, क्षेत्र, दंगे, और वादों की टालमटोल से बनते हैं। सत्ता एक सेवा नहीं, धंधा बन गई है — जहाँ टिकट बिकते हैं, नीतियाँ गिरवी रखी जाती हैं, और जनमत केवल एक “चुनावी आँकड़ा” रह जाता है। हमने नीतियों की जगह घोषणाएँ, और विकास की जगह वोट बैंक को प्राथमिकता दी।
स्कूलों में नैतिक शिक्षा की जगह चुनावी रणनीतियाँ आ गईं।
किसान, मजदूर, शिक्षक — जो देश का आधार थे, उन्हें केवल समस्या माना जाने लगा। ये सब नेतागिरी की देन है — जिसमें सत्ता का मोह, सेवा की भावना को निगल गया।
1. राजनीति — एक सेवा से कैसे बन गई निजी सत्ता का खेल?
भारत के स्वतंत्र होते ही हमें एक ऐतिहासिक मौका मिला था — राष्ट्र को न्याय, शिक्षा, समता और समृद्धि की राह पर ले जाने का।
परंतु सेवा का यह व्रत शीघ्र ही राजतंत्र की नकल में बदल गया।
राजनीति, जो पहले जन-हित की नीतियाँ बनाती थी, अब "नेतागिरी" बन गई जो केवल सत्ता और प्रचार की भूख से संचालित होती है।
संसद की गरिमा टीवी डिबेट की चीखों में गुम हो गई।
जनता के मुद्दे चुनावी नारों में खो गए।
और नेतृत्व का आदर्श व्यक्तिपूजा और ब्रांडिंग बन कर रह गया।
भारत के बुनियादी मुद्दों (शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, रोज़गार) पर ध्यान कम, और मूर्ति, मजार, मंदिर-मस्जिद की बहसों पर ध्यान अधिक हो गया।
2. नीति नहीं, केवल चुनावी रणनीति: देश का दीर्घकालीन नुकसान
भारत में अधिकतर सरकारें पाँच वर्षों के कार्यकाल को सिर्फ़ अगले चुनाव की तैयारी के रूप में देखती हैं।
"दूरदृष्टि" की जगह "अल्पकालिक जीत" का मोह निर्णयों को प्रभावित करता है।
गांवों के विकास की नीतियाँ केवल कागज़ पर बनती हैं, ज़मीन पर ठेकेदारऔर कमीशनखोर हावी होते हैं।
कृषि सुधार या तो अधूरे रहते हैं, या सिर्फ़ नारे बनकर रह जाते हैं।
शिक्षा प्रणाली को ज्ञान का केंद्र बनाने के बजाय कोचिंग और प्राइवेट स्कूल माफिया को सौंप दिया गया।
जब नीति केवल चुनाव जिताने के लिए बने, तो समाज केवल वोट बैंक बन जाता है — और राष्ट्र की आत्मा खो जाती है।
3. भ्रष्टाचार — एक अनदेखा लेकिन सर्वव्याप्त दानव
भारत में हर बड़ी योजना के साथ एक "घोटाले" की आशंका जुड़ी होती है — जैसे यह कोई परंपरा हो।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज चोरी,
बिजली और सड़क परियोजनाओं में भ्रष्टाचार,
स्वास्थ्य और टीकाकरण योजनाओं में झोलाछाप व्यवस्था...
यह सब केवल पैसे की बात नहीं है — यह जन-विश्वास के टूटने की बात है। जब नागरिक को लगता है कि हर सिस्टम उसके खिलाफ है, तो वह भी नियमों को तोड़ना अपना हक़ समझता है।
यह भ्रष्टाचार केवल नेताओं तक सीमित नहीं — यह अब एक संस्कृति बन चुकी है।
4. शिक्षा — विचारशील नागरिक नहीं, सिर्फ़ कर्मचारी बना रही है
हमारे गुरुकुलों ने शंकराचार्य, चाणक्य, और तुलसीदास जैसे विचारक दिए पर आज की शिक्षा प्रणाली सिर्फ़ डिग्री और नौकरी देने में सिमट गई है। चिंतन, आत्म-अनुशासन, समाजबोध की जगह अब केवल MCQ और स्कोर बोर्ड की दौड़ है। सरकारी स्कूलों की दशा ऐसी कि वहां पढ़ने वाला बच्चा स्वयं को हीन समझने लगता है। जब शिक्षा ही व्यक्ति को "राष्ट्र का भागीदार" नहीं बनाती, तब लोकतंत्र खोखला हो जाता है।
5. भारत की आत्मा — किसान, कारीगर, मज़दूर — सबसे उपेक्षित
हमारा संविधान कहता है: भारत गांवों का देश है।
लेकिन असल सच्चाई यह है कि:
किसान आत्महत्या कर रहा है,
कारीगर सस्ते चीनी उत्पादों से हारा बैठा है,
मज़दूर शहरों में दिहाड़ी और अपमान के बीच पिसता है।
और ये सब तब हो रहा है जब हमारे पास सब कुछ है — सिर्फ़
नीति और नीयत की ईमानदारी नहीं है।
उपसंहार:
नेतृत्व का पतन, जनशक्ति का मौन
भारत की सबसे बड़ी ताक़त है — उसकी जनशक्ति।
पर यह जनशक्ति नेतागिरी के शोर में मौन हो गई है।
पर याद रखना मित्रों:
“अगर राष्ट्र का भाग्य सो गया है, तो उसे जगाने का काम केवल जनता ही कर सकती है।”
भारत को नेतृत्व की नहीं, जनचेतना की क्रांति की ज़रूरत है।